एक के बाद आती आपदाओं के बीच एक ख़बर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की आती है और कुहासा थोड़ा और बढ़ने लगता है. उनकी मौत के पीछे के कारणों में हिंदी सिनेमा संसार में पहले से स्थापित कैम्प या गिरोह या गुटों द्वारा इस बाहर से आयातित एक्टर की सायास अवहेलना और दरकिनार करने की ओछी राजनीति सामने आती है. अभी क़यास हैं, साबित कुछ भी नहीं है. होगा? शायद कभी नहीं.
लेकिन जिन्हें इस परिघटना पर आश्चर्य है उनके आश्चर्य पर आश्चर्य किया जा सकता है. दरअसल गुटबाजी च गिरोहबंदी च ओछी राजनीति हमारा मूल चरित्र है. हमारी व्यावहारिक सामाजिकता. वे ऑफ लाइफ, यू नो.
सिनेमा के अन्य अंग-उपांग इससे अछूते हैं क्या? बहुत से ऐसे शानदार गायक रहे जिन्हें संगीतकारों ने अपने कैम्प का न होने की वजह से गाने नहीं दिए, यही संगीतकारों के साथ भी हुआ, निर्देशकों के साथ भी और अलां-फलां कलाओं में माहिर कलाकारों के साथ भी. ये चरित्र सिर्फ सिनेमा तक ही महदूद है? ना!
किसी सरकारी नौकर से पूछिए. किस तरह की छिपी और खुली गिरोहबंदी ऊपर के पदों से लेकर नीचे तक हमेशा रहती है. कैसे किसी कार्मिक की पोस्टिंग के निर्णय से लेकर उसके रोजमर्रा के भी बहुत से काम गुटबाज़ियो के तहत प्रभावित होते हैं. कैसे आपके सरकारी नौकरी की दहलीज पर पाँव धरते ही ‘मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ’ का लकीर प्रश्न स्वागत करता है.
‘निजी संस्थान, मल्टी नेशनल कम्पनी तो विशुद्ध रूप से मुनाफ़े पर काम करती है दस इन ग़ैर सरकारी नौकरी प्रोफेशनलिज़्म प्रीवेल्स’ अगर आप ये सोच रहे हैं तो पूछिये अपने भाई बंधुओं से, उनकी काम की क़ाबिलियत और शक्ति केंद्र की चापलूसी की क़ाबिलियत में कौन सी ज़्यादा कारगर रही?
कोई ऐसा पेशा नहीं है जिसमें गिरोहबंदी न हो. वक़ालत-अदालत (चुप-चुप कंटेम्प्ट चुप्प!)
मीडिया तो गढ़ है शक्ति केंद्रों का. यहाँ शक्ति केंद्रों के शक्ति केंद्र हैं. किसी लोकल-वोकल या नेशनल-रेशनल (प्लेयिंग विद वर्ड्स. डोंट टेक इट सीरियसली, इवेन द प्रीवियस वन) अख़बार या चैनल में घुस के उनकी फील्ड रिपोर्टर से एडिटिंग टेबल तक देख लीजिए. अट्ठारह सफहों के अख़बार के दफ़्तर में गुटबाज़ियो की छत्तीस लेयर्स होती हैं.
राजनीति तो खुल्ली (आधा ल मामे की शादी में नहीं आया है उसका अपना एटीट्यूड है) गिरोहबंदी है. गिरहबन्दी भी. ना! मैं राजनैतिक दलों की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं उन दलपुंजो में शामिल पुंकेसर और स्त्रीकेसर की बात कर रहा हूँ. आंतरिक लोकतंत्र चाल, चरित्र और चेहरे के सरलीकृत जुमले से नहीं बल्कि जोर-जुगाड़ और जम जमाव से चलता है.
और नीचे उतरिये. परिवार में, आस-पड़ोस, मुहल्ले और करीबी समाज में छोटे-छोटे शक्ति-स्थल बन ही जाते हैं. पर्दे के रंग वही भाई डिसाइड करता है जो थोड़ा ज्यादा कमाता है या याँ-वां थोड़ी पहुंच रखता है.
‘ओ ईजा’ ऊब कर एक मेरिट धारी (दर्जा धारी नहीं उसका तो प्रभार ही इस डिस्कोर्स का शिलालेख है) मानुस सांसारिक गुटबाज़ियो से सन्यास लेने की सोच सकता है. लेकिन ‘मठाधीश’ शब्द के उत्पत्ति स्थल पर तो सबसे मौलिक गिरोहबंदी है. मेरी माँ हमेशा कहा करती हैं ‘छूछे के के पूछे’ यानि जिसके पास कुछ नहीं है न धन दौलत, न मठाधीशी, न ही पॉवर कनेक्शन उसको कौन पूछेगा? सन्यास लेने के लिए भी आपको संघम शपथ लेनी पड़ती है.
दरअसल मेरिट क्या होती है हम नहीं जानते. व्यक्ति की गरिमा से हमें कोई लेना-देना नहीं है. हमारी सामाजिकता बुरी तरह से ‘टूटी हुई-बिखरी हुई’ है. जो सिर विरोध में उठे हैं थोड़ा थम कर दुबारा देखिये, वो भी अपना परचम लिए खड़े हैं. उनकी बांह पर भी बिल्ला है. अगर नहीं है तो थोड़ी देर और थामिए खुद को. दूसरे खेमे में सटर-पटर होने लगी है. उसके लिए आसन बनाए जा रहे हैं. उसे अपने जैसा दिखने के अंदरूनी मुखौटे तैयार हो रहे हैं. अभी बयान आने वाला है कि फलाने मियाँ दरअसल हमारी ही सन्तान हैं.
हम कभी खुद से पूछने की ताब हासिल कर पाएंगे? तब तक जाने कौन सा सुशांत…
ख़ैर! सुना है फेसबुक लाइव और पोस्ट डेड के माध्यम से हिंदी साहित्य (कविता) की ओछी राजनीति, गुटबाज़ी और गिरोहबंदी के आरोपों-प्रत्यारोपों की बहस खासी चल निकली है. मगर हम चुप रहेंगे. वैसे भी हमारा बोलना सुनेगा भी कौन? छूछे के, के पूछे?





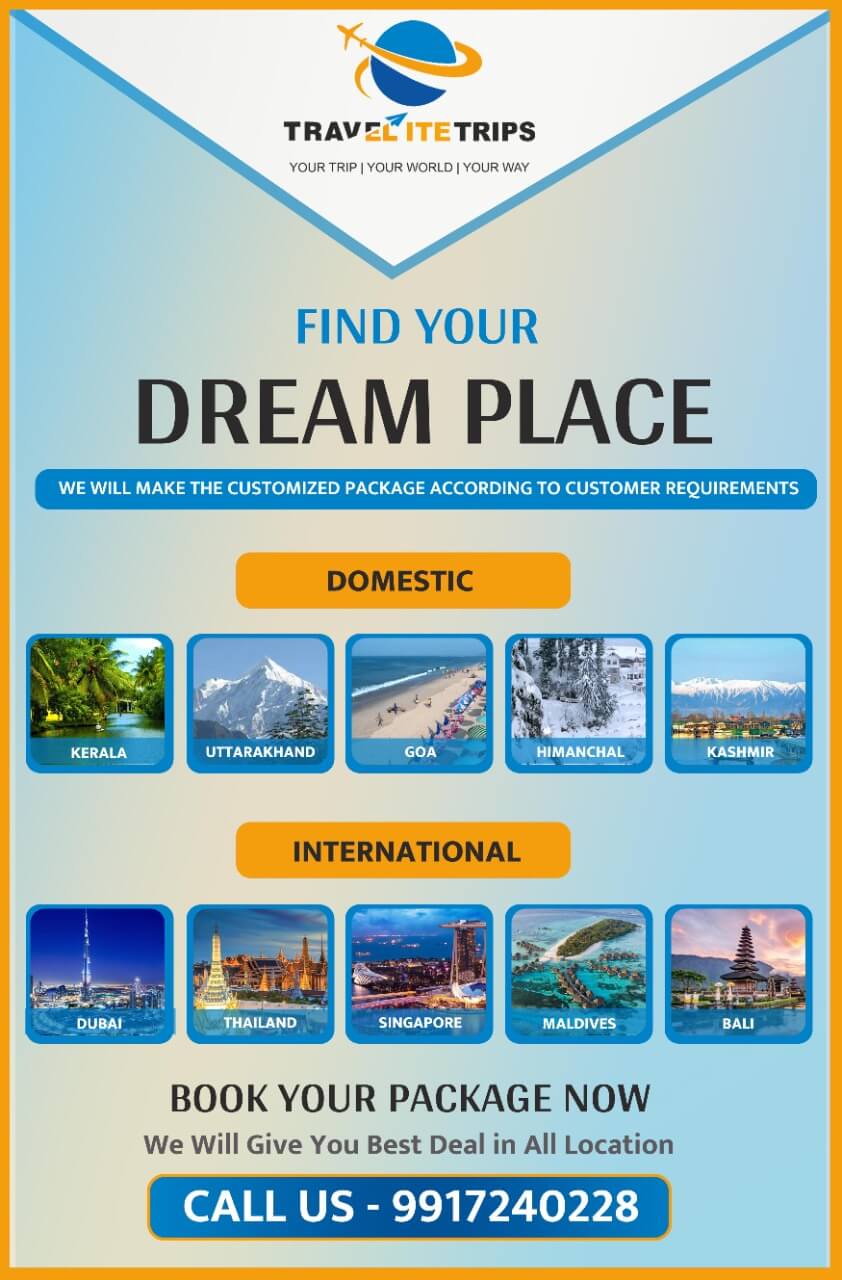

अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें

 उत्तराखंड – वोटर कार्ड के अलावा 12 अन्य दस्तावेजों से हो सकता है मतदान
उत्तराखंड – वोटर कार्ड के अलावा 12 अन्य दस्तावेजों से हो सकता है मतदान  उत्तराखंड- प्रदेश में चार धाम यात्रा के लिए हेली टिकटों की बुकिंग 20 अप्रैल से होगी शुरू
उत्तराखंड- प्रदेश में चार धाम यात्रा के लिए हेली टिकटों की बुकिंग 20 अप्रैल से होगी शुरू  हल्द्वानी -(बड़ी खबर) मतदान दिवस यानी कल आवश्यक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं
हल्द्वानी -(बड़ी खबर) मतदान दिवस यानी कल आवश्यक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं  देहरादून -(बड़ी खबर) कल छोटे बड़े सभी अस्पताल खोलने के निर्देश
देहरादून -(बड़ी खबर) कल छोटे बड़े सभी अस्पताल खोलने के निर्देश  देहरादून -(बड़ी खबर) मतदान को लेकर कल की छुट्टी के निर्देश
देहरादून -(बड़ी खबर) मतदान को लेकर कल की छुट्टी के निर्देश  हल्द्वानी -हल्द्वानी MBPG से पोलिंग पार्टियां रवाना, 33सौ सुरक्षा कर्मचारी, 7 कंपनी CAPF, 2 कंपनी PAC तैनात
हल्द्वानी -हल्द्वानी MBPG से पोलिंग पार्टियां रवाना, 33सौ सुरक्षा कर्मचारी, 7 कंपनी CAPF, 2 कंपनी PAC तैनात  उत्तराखंड – यहां बाघ ने उतारा ग्रामीण को मौत घाट, मचा हड़कंप
उत्तराखंड – यहां बाघ ने उतारा ग्रामीण को मौत घाट, मचा हड़कंप  उत्तराखंड: पिता बेचते हैं चाय, मेहनती बिटिया ने UPSC कर लिया क्वालीफाई
उत्तराखंड: पिता बेचते हैं चाय, मेहनती बिटिया ने UPSC कर लिया क्वालीफाई  उत्तराखंड – रानीखेत के बिंता गांव निवासी दिपेश कैड़ा बने IAS, गांव में हर जगह जश्न ही जश्न
उत्तराखंड – रानीखेत के बिंता गांव निवासी दिपेश कैड़ा बने IAS, गांव में हर जगह जश्न ही जश्न  हल्द्वानी -(बड़ी खबर) यहां से तीन बच्चे अचानक लापता
हल्द्वानी -(बड़ी खबर) यहां से तीन बच्चे अचानक लापता 